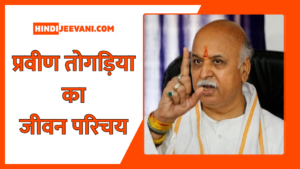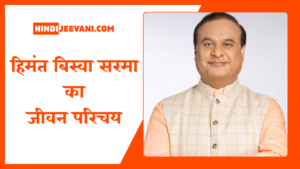मुंशी प्रेमचंद (31 जुलाई 1880 – 8 अक्टूबर 1936) हिंदी और उर्दू साहित्य के सबसे प्रभावशाली और सम्मानित लेखकों में से एक थे। उनका जन्मनाम धनपत राय श्रीवास्तव था, लेकिन साहित्यिक जगत में वे “प्रेमचंद” के नाम से प्रसिद्ध हुए। हिंदी साहित्य में Munshi Premchand “उपन्यास सम्राट” की उपाधि से नवाजा गया है। प्रेमचंद की रचनाएँ यथार्थवाद की परिचायक हैं, जो भारतीय समाज की गहराइयों, उसकी कुरीतियों, गरीबी, शोषण और मानवीय संवेदनाओं को उजागर करती हैं। उनकी लेखनी ने सामाजिक जागरूकता और सुधार को बढ़ावा दिया, जिसके कारण वे केवल एक लेखक ही नहीं, बल्कि एक समाज सुधारक के रूप में भी याद किए जाते हैं। उनकी प्रमुख कृतियों में गोदान, गबन, निर्मला, रंगभूमि और ईदगाह जैसी रचनाएँ शामिल हैं, जो आज भी साहित्य प्रेमियों के बीच लोकप्रिय हैं। प्रेमचंद ने अपने लेखन के जरिए हिंदी और उर्दू साहित्य को एक नई ऊँचाई दी और भारतीय साहित्य को विश्व पटल पर पहचान दिलाई।
मुंशी प्रेमचंद का प्रारंभिक जीवन
मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के लमही गाँव में हुआ था। उनका जन्म एक मध्यमवर्गीय कायस्थ परिवार में हुआ था, जहाँ उनके माता-पिता की सादगी और मेहनत ने उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। Munshi Premchand के पिता अजायब राय डाक विभाग में एक साधारण क्लर्क थे। अजायब राय की आय बहुत सीमित थी, और वे अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए कठिन परिश्रम करते थे। उनकी मेहनत और ईमानदारी प्रेमचंद के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी, हालाँकि आर्थिक तंगी ने परिवार को हमेशा परेशान रखा। उनकी माता आनंदी देवी एक धार्मिक, सौम्य और ममता से भरी महिला थीं। आनंदी देवी अपने बच्चों की परवरिश में पूरी तरह समर्पित थीं और प्रेमचंद के प्रति उनका विशेष स्नेह था। उनकी सादगी और धार्मिकता ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व को संवेदनशील बनाया। लेकिन जब प्रेमचंद केवल सात साल के थे, तब उनकी माँ का असामयिक निधन हो गया। यह घटना उनके जीवन का सबसे दुखद मोड़ थी, जिसने उनके मन पर गहरी छाप छोड़ी। माँ की मृत्यु के बाद अजायब राय ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन प्रेमचंद का अपनी सौतेली माँ के साथ रिश्ता कभी भी मधुर नहीं बन सका। सौतेली माँ का व्यवहार उनके प्रति कठोर था, जिसके कारण उनके बचपन में भावनात्मक शून्यता आ गई। यह शून्यता और पारिवारिक तनाव उनकी रचनाओं में बार-बार झलकता है, खासकर गरीब और उपेक्षित पात्रों के चित्रण में।
प्रेमचंद की प्रारंभिक शिक्षा उनके गाँव लमही में शुरू हुई। वे एक होनहार छात्र थे और 13 साल की उम्र में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। इसके बाद वे आगे की पढ़ाई के लिए बनारस (अब वाराणसी) गए और क्वींस कॉलेज में दाखिला लिया। लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि उन्हें पढ़ाई छोड़कर नौकरी शुरू करनी पड़ी। अजायब राय चाहते थे कि उनका बेटा पढ़-लिखकर एक अच्छी नौकरी हासिल करे, ताकि परिवार का भविष्य सुरक्षित हो सके। हालाँकि, पिता का स्वास्थ्य भी धीरे-धीरे बिगड़ता गया और उनकी मृत्यु तब हुई जब Munshi Premchand अभी युवावस्था में थे। पिता के निधन के बाद परिवार की जिम्मेदारियाँ उनके कंधों पर आ गईं। फिर भी, उन्होंने हार नहीं मानी और नौकरी के साथ-साथ आत्मशिक्षा जारी रखी। कठिन परिश्रम के बल पर उन्होंने बी.ए. की डिग्री हासिल की, जो उस समय उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि थी।
मुंशी प्रेमचंद का करियर
प्रेमचंद ने अपने करियर की शुरुआत 1899 में एक स्कूल मास्टर के रूप में की। उस समय उनकी मासिक आय केवल 20 रुपये थी, जो परिवार चलाने के लिए नाकाफी थी। वे छोटे-छोटे गाँवों में पढ़ाने के लिए नियुक्त किए गए, जहाँ उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें सम्मान दिलाया। धीरे-धीरे वे शिक्षा विभाग में सब-डिप्टी इंस्पेक्टर के पद तक पहुँचे। इस नौकरी ने Munshi Premchand कुछ आर्थिक स्थिरता दी, लेकिन उनकी आत्मा इसमें संतुष्ट नहीं थी। 1921 में, जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, प्रेमचंद इससे गहरे रूप से प्रभावित हुए। उन्होंने अंग्रेजी सरकार की नीतियों के खिलाफ अपनी असहमति जताते हुए सरकारी नौकरी छोड़ दी। यह निर्णय उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि इसके बाद वे पूर्णकालिक लेखक बन गए। नौकरी छोड़ने के बाद उनकी आर्थिक स्थिति और खराब हो गई, लेकिन उनकी साहित्यिक प्रतिबद्धता कभी कम नहीं हुई।
प्रेमचंद ने लेखन के साथ-साथ प्रकाशन और संपादन के क्षेत्र में भी योगदान दिया। 1930 में उन्होंने “हंस” नामक साहित्यिक पत्रिका शुरू की, जो हिंदी साहित्य के विकास में मील का पत्थर साबित हुई। “हंस” के माध्यम से उन्होंने न केवल अपनी रचनाएँ प्रकाशित कीं, बल्कि नए लेखकों को भी मंच प्रदान किया। इसके अलावा, वे “जागरण” नामक पत्रिका के संपादक भी रहे। अपने प्रकाशन कार्य को आगे बढ़ाने के लिए Munshi Premchand ने “सरस्वती प्रेस” की स्थापना की, जिसके जरिए उनकी कई रचनाएँ और अन्य लेखकों के कार्य प्रकाशित हुए। हालाँकि, प्रकाशन का यह व्यवसाय आर्थिक रूप से बहुत सफल नहीं रहा और वे कर्ज में डूबते चले गए। फिर भी, प्रेमचंद ने कभी साहित्यिक मूल्यों से समझौता नहीं किया।
मुंशी प्रेमचंद का लेखन और साहित्यिक योगदान
प्रेमचंद ने अपने साहित्यिक करियर की शुरुआत उर्दू भाषा में की, क्योंकि उस समय उर्दू उत्तर भारत में व्यापक रूप से प्रचलित थी। उनका पहला उर्दू उपन्यास असरार-ए-मआबिद 1903 में प्रकाशित हुआ, जिसे बाद में हिंदी में देवस्थान रहस्य के नाम से पुनर्प्रकाशित किया गया। शुरू में वे “नवाब राय” के नाम से लिखते थे। उनका पहला कहानी संग्रह सोज-ए-वतन 1907 में प्रकाशित हुआ, जिसमें देशभक्ति की भावना थी। इस संग्रह को ब्रिटिश सरकार ने देशद्रोही मानकर जब्त कर लिया और उन पर साहित्यिक प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद उन्होंने “प्रेमचंद” नाम अपनाया और हिंदी साहित्य में अपनी पहचान बनाई। उनकी लेखन शैली बेहद सरल, सहज और यथार्थवादी थी। Munshi Premchand जटिल साहित्यिक भाषा के बजाय आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग करते थे, जिससे उनकी रचनाएँ जन-जन तक पहुँचीं।
Munshi Premchand के प्रमुख उपन्यासों में सेवासदन (1919) शामिल है, जो वेश्याओं की दयनीय स्थिति पर आधारित है। प्रेमाश्रम (1922) में ग्रामीण जीवन और जमींदारी व्यवस्था की समस्याओं को उठाया गया। रंगभूमि (1925) एक अंधे भिखारी सूरदास की संघर्ष गाथा है, जो समाज की असमानता को दर्शाती है। कायाकल्प (1926) और निर्मला (1927) में दहेज प्रथा और महिलाओं के शोषण जैसे मुद्दों पर प्रकाश डाला गया। गबन (1931) में भ्रष्टाचार और नैतिक पतन की कहानी है, जबकि कर्मभूमि (1932) स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक सुधार की पृष्ठभूमि पर आधारित है। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति गोदान (1936) है, जो भारतीय किसानों की गरीबी, शोषण और सामाजिक असमानता का मार्मिक चित्रण करती है। उनकी कहानियाँ भी उतनी ही प्रभावशाली हैं। ईदगाह में एक बच्चे का त्याग और मासूमियत, नमक का दारोगा में ईमानदारी की जीत, पूस की रात में किसान की मजबूरी, और कफन में गरीबी का काला पक्ष दिखाया गया है। शतरंज के खिलाड़ी उनकी ऐतिहासिक कहानी है, जो अवध के नवाबों की विलासिता और पतन को चित्रित करती है।
प्रेमचंद की रचनाओं में सामाजिक कुरीतियों जैसे जातिवाद, दहेज प्रथा, विधवा विवाह, और महिलाओं के शोषण पर गहरी चोट की गई है। वे समाज के निम्न और मध्यम वर्ग की आवाज बने और Munshi Premchand की पीड़ा को अपनी लेखनी में उतारा। उनकी रचनाएँ केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि समाज को जागृत करने का साधन थीं।
मुंशी प्रेमचंद का व्यक्तिगत जीवन
प्रेमचंद की पहली शादी कम उम्र में हुई थी, जिसे उनके परिवार ने तय किया था। यह विवाह असफल रहा और जल्द ही टूट गया। इसके बाद उन्होंने शिवरानी देवी से दूसरी शादी की, जो एक विधवा थीं। उस समय के रूढ़िवादी समाज में यह एक साहसिक और क्रांतिकारी कदम था। शिवरानी Munshi Premchand के लेखन और विचारों की समर्थक बनीं और उनके साथ उनका रिश्ता मजबूत रहा। उनके दो पुत्र, श्रीपत राय और अमृत राय, और एक पुत्री, कमला देवी, थे। प्रेमचंद का पारिवारिक जीवन आर्थिक संकटों से जूझता रहा। लेखन और प्रकाशन से होने वाली आय बहुत कम थी, और वे जीवनभर कर्ज में डूबे रहे। परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए उन्होंने कठिन मेहनत की, लेकिन उनकी सादगी और साहित्यिक प्रतिबद्धता कभी कम नहीं हुई।
मुंशी प्रेमचंद की मृत्यु और विरासत
लंबी बीमारी के बाद 8 अक्टूबर 1936 को प्रेमचंद का निधन हो गया। उनके अंतिम दिन कष्टमय थे, और वे उस समय मंगलसूत्र नामक उपन्यास पर काम कर रहे थे, जो अधूरा रह गया। उनकी मृत्यु हिंदी साहित्य के लिए एक बड़ी क्षति थी। प्रेमचंद की रचनाओं का अंग्रेजी, रूसी, फ्रेंच सहित कई भाषाओं में अनुवाद हुआ, जिससे उनकी ख्याति अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैली। उनकी लेखनी ने हिंदी साहित्य को नई दिशा दी और उसे जन-जन तक पहुँचाया। आज भी Munshi Premchand की रचनाएँ पाठकों को प्रेरित करती हैं और सामाजिक चेतना जागृत करती हैं। उन्हें हिंदी साहित्य का “उपन्यास सम्राट” कहा जाता है, और उनकी विरासत नई पीढ़ी के लिए एक अमूल्य धरोहर है।
मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख रचनाएँ
- उपन्यास: सेवासदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान।
- कहानी संग्रह: सप्त सरोज, नवनिधि, प्रेम पचीसी, मानसरोवर (8 खंड)।
- प्रसिद्ध कहानियाँ: ईदगाह, नमक का दारोगा, पूस की रात, कफन, शतरंज के खिलाड़ी।
- नाटक और निबंध: संघर्ष, कर्बला, विभिन्न समसामयिक लेख।
मुंशी प्रेमचंद का प्रभाव और सम्मान
प्रेमचंद का प्रभाव हिंदी और उर्दू साहित्य पर गहरा रहा। उनकी रचनाएँ साहित्यिक पाठ्यक्रमों का हिस्सा हैं और कई फिल्मों, नाटकों और धारावाहिकों में रूपांतरित हुई हैं। Munshi Premchand की कहानी शतरंज के खिलाड़ी पर सत्यजीत राय ने एक प्रसिद्ध फिल्म बनाई। प्रेमचंद ने साहित्य को समाज का दर्पण बनाया और उसे जनसामान्य की आवाज दी। उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी रचनाएँ जीवित हैं और समाज को दिशा दिखा रही हैं।